राजनीतिकी विश्वस्तरपर सर्वसम्मत परिभाषा

“सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सम्पन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाजकी संरचना राजनीतिकी मन्वादि धर्मशास्त्रसम्मत विश्वस्तरपर सर्वसम्मत सार्वभौम परिभाषा है।”
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या ३२
कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठ:
कालेनान्यस्तस्य मूलं हरेत कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठ:।।
(महाभारत – शान्तिपर्व १२०. ३९)

“शत्रु बाल, युवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, सदा सावधान न रहनेवाले मनुष्यका नाश कर डालता है। अन्य कोई धनसम्पन्न शत्रु अनुकूल समयका सहयोग पाकर राजाकी जड़ उखाड़ सकता है। अत एव जो समयको जानता है, वही राजाओं में श्रेष्ठ है।।“
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २३०
षड्गुण
सन्धिश्च विग्रहश्चैव यानमासनमेव च।
द्वैधीभाव: संश्रयश्च षड्गुणा: परिकीर्त्तिता:।।
(महाभारत – शान्तिपर्व २३४. १७)
“किसी शर्तपर समकक्ष या प्रबल शत्रुसे सामञ्जस्य ‘सन्धि’ है। युद्धादिके द्वारा उसे हानि पहुँचाना ‘विग्रह’ है। विजयाभिलाषी राजा जो शत्रुके ऊपर चढ़ाई करता है, वह यात्रा या ‘यान’ है। विग्रह छेड़कर अपने ही देशमें रहना ‘आसन’ है। आधी सेनाको किलेमें छिपाकर आधी सेनाके साथ युद्धकी भावनासे यात्रा करना ‘द्वैधीभाव’ है। असमर्थताकी दशामें लाभकी सम्भावना होने पर उदासीन अथवा मध्यम राजाकी शरणागति ‘संश्रय’ है।“
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २२८
बुद्धे: पश्चात् कर्म यत्तत् प्रशस्तम्
प्रत्यक्षेणानुमानेन तथौपम्यागमैरपि।
परीक्ष्यास्ते महाराज स्वे परे चैव नित्यश:।।
(महाभारत — शान्तिपर्व ५६. ४१)
“महाराज ! प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम — इन चारों प्रमाणोंके द्वारा सदा अपने – परायेकी पहचान करते रहना चाहिये।।”
प्रत्यक्षनुमानं च सर्वेषां योनिरिष्यते।
प्रमाणज्ञो हि शक्नोति दण्डनीतौ विचक्षण:।।
अप्रमाणवतां नीतो दण्डो हन्यान्महीपतिम्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २४. दा०)
“इनमेंसे प्रत्यक्ष और अनुमान — ये दो सबके लिये निर्णयके आधार माने गये हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणोंको जाननेवाला पुरुष दण्डनीतिमें कुशल हो सकता है। जो प्रमाणशून्य हैं, उनके द्वारा प्रयोगमें लाया गया दण्ड राजाका विनाश कर सकता है।।”

तर्कशास्त्रकृता बुद्धिर्धर्मशास्त्रकृता च या।
दण्डनीतिकृता चैव त्रैलोक्यमपि साधयेत्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २४. दा०)
“तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दण्डनीतिसे परिष्कृत — बुद्धि तीनों लोकोंकी भी सिद्धि कर सकती है।।”
आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतिषु पारगा:।
ते तु सर्वत्र योक्तव्यास्ते च बुद्धे: परं गता:।
गुणयुक्त्तेऽपि नैकस्मिन् विश्वसेत विचक्षण:।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २४. १८)
“आन्विक्षिकी (वेदान्त), वेदत्रयी, वार्ता तथा दण्डनीतिके जो पारङ्गत विद्वान् हों, उन्हें सब कार्योंमें नियुक्त करना चाहिये; क्योंकि वे बुद्धिकी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए होते हैं। एक व्यक्ति कितना ही गुणवान् क्यों न हों, विद्वान् पुरुषको केवल उसपर विश्वास कर उसीके भरोसे नहीं रहना चाहिये।।”
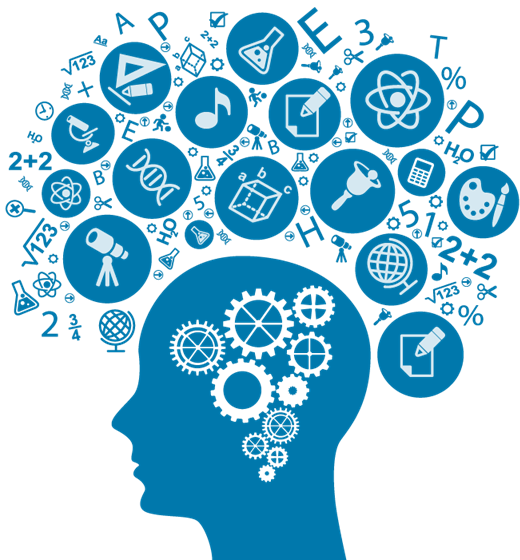
बुद्धिर्दीप्ता बलवन्तं हिनस्ति बलं बुद्ध्या पाल्यते वर्धमानम्।
शत्रुर्बुद्ध्या सीदते वर्धमानॊ बुद्धेः पश्चात् कर्म यत्तत् प्रशस्तम्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व १२०. ४२)
“प्रतिभाशालिनी बुद्धि बलवान् को भी पछाड़ देती है। बुद्धिके द्वारा नष्ट होते हुए बलकी भी रक्षा होती है। बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धिके द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है। बुद्धिसे सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है, वह सर्वोत्तम है।।”
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २२२-२२४
विपत्तिस्थस्य राज्ञः कर्तव्यानां वर्णनम्
परचक्राभियातस्य दुर्बलस्य बलीयसा।
आपन्नचेतसॊ ब्रूहि किं कार्यमवशिष्यते।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ३)
“जिसपर शत्रुदलका आक्रमण हो गया हो, जो दुर्बल होकर बलवान शत्रुके द्वारा पीड़ित हो और विपत्तिमें पड़कर जिसका चित्त घबरा उठा हो, उसके लिये कौन-सा कार्य शेष रह जाता है? — उसे इस संकटसे मुक्त होनेके लिये क्या करना चाहिये? ।।”
बाह्यश्चेद् विजिगीषुः स्याद् धर्मार्थकुशलः शुचिः।
जवेन संधिं कुर्वीत पूर्वभुक्तान् विमॊचयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ४)
“राजन ! यदि विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाला राजा बाहरका हो, उसका आचार-विचार शुद्ध हो तथा वह धर्म और अर्थके साधनमें कुशल हो तो शीघ्रतापूर्वक उसके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये और जो ग्राम तथा नगर अपने पूर्वजोंके धिकारमें रहे हों, वे यदि आक्रमणकारीके हाथमें चले गये हों तो उसे मधुर वचनोंद्वारा समझा-बुझाकर उसके हाथसे छुड़ानेकी चेष्टा करे।।”

योऽधर्मविजिगीशु: स्याद् बलवान् पापनिश्चयः।
आत्मनः संनिरॊधेन संधिं तेनापि रोचयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ५)
“जो विजय चाहनेवाला शत्रु अधर्मपरायण हो तथा बलवान होनेके साथ ही पापपूर्ण विचार रखता हो, उसके साथ अपना कुछ खोकर भी सन्धि कर लेनेकी ही इच्छा रखे।।”
अपास्य राजधानीं वा तरेद् द्रव्येण चापदम्।
तद्भावयुक्तो द्रव्याणि जीवन् पुनरुपार्जयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ६)
“अथवा आवश्यकता हो तो अपनी राजधानीको भी छोड़कर बहुत-सा द्रव्य देकर उस विपत्तिसे पार हो जाय। यदि वह जीवित रहे तो राजोचित गुणसे युक्त होनेपर पुनः धनका उपार्जन कर सकता है।।”

अवरॊधान् जुगुप्सेत का सपत्नधने दया।
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथंचन।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ८)
“शत्रुका आक्रमण हो जानेपर राजाको सबसे पहले अपने अन्तःपुरकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये। यदि वहाँ शत्रुका अधिकार हो जाय, तब उधरसे अपनी मोह-ममता हटा लेनी चाहिये; क्योंकि शत्रुके अधिकारमें गये हुए धन और परिवारपर दया दिखाना किस कामका? जहाँतक सम्भव हो, अपने-आपको किसी तरह भी शत्रुके हाथमें नहीं फँसने देना चाहिये।।”
आभ्यन्तरे प्रकुपिते बाह्ये चॊपनिपीडिते।
क्षीणे कॊशे श्रुते मन्त्रे किं कार्यमवशिष्यते।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ९)
“पितामह! यदि बाहर राष्ट्र और दुर्ग आदिपर आक्रमण करके शत्रु उसे पीड़ा दे रहे हों और भीतर मन्त्री आदि भी कुपित हों, खजाना खाली हो गया हो और राजाका गुप्त रहस्य सबके कानोंमें पड़ गया हो, तब उसे क्या करना चाहिये? ।।”

क्षिप्रं वा संधिकामः स्यात् क्षिप्रं वा तीक्ष्णविक्रमः।
तदापनयनं क्षिप्रमेतावत् साम्परायिकम्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १०)
“राजन्! उस अवस्थामें राजा या तो शीघ्र ही सन्धिका विचार कर ले अथवा जल्दी-से-जल्दी दुःसह पराक्रम प्रकट करके शत्रुको राज्यसे निकाल बाहर करे, ऐसा उद्योग करते समय यदि कदाचित् मृत्यु भी हो जाय तो वह परलोकमें मंगलकारी होती है।।”
अनुरक्तेन चेष्टेन हृष्टेन जगतीपति:।
अल्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति भूमिप:।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ११)
“यदि सेना स्वामीके प्रति अनुराग रखनेवाली, प्रिय और हृष्ट-पुष्ट हो तो उस थोड़ी-सी सेनाके द्वारा भी राजा पृथ्वीपर विजय पा सकता है।।”

हतॊ वा दिवमारॊहेद्धत्वा वा क्षितिमावसेत्।
युद्धे हि संत्यजन् प्राणान् शक्रस्यैति सलॊकताम्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १२)
“यदि वह युद्धमें मारा जाय तो स्वर्गलोकके शिखरपर आरूढ़ हो सकता है अथवा यदि उसीने शत्रुको मार लिया तो वह पृथ्वीका राज्य भोग सकता है। जो युद्धमें प्राणोंका परित्याग करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है।।”
सर्वलॊकागमं कृत्वा मृदुत्वं गन्तुमेव च।
विश्वासाद् विनयं कुर्याद् विश्वसेच्चाप्युपायत:।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १३)
“अथवा दुर्बल राजा शत्रुमें कोमलता लानेके लिये विपक्षके सभी लोगोंको संतुष्ट करके उनके मनमें विश्वास जमाकर उनसे युद्ध बंद करनेके लिये अनुनय-विनय करे और स्वयं भी उपायपूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे।।”

अपचिक्रमिषु: क्षिप्रं साम्ना वा परिसान्त्वयन्।
विलङ्घयित्वा मन्त्रेण ततः स्वयमुपक्रमेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १४)
“अथवा वह मधुर वचनोंद्वारा विरोधी दलके मन्त्री आदिको प्रसन्न करके दुर्गसे पलायन करनेका प्रयत्न करे। तदनन्तर कुछ काल व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति ले अपनी खोयी हुई सम्पत्ति अथवा राज्यको पुनः प्राप्त करनेका प्रयत्न आरम्भ करे।।”
(महाभारत – शान्तिपर्व १३१-वाँ अध्याय)
राज्यं पण्यं न कारयेत्
तरसा बुद्धिपूर्वं वा निग्राह्या एव शत्रव:।
पापै: सह न संदध्याद् राज्यं पण्यं न कारयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व २४. १६)
“शत्रुओंको बल
और बुद्धिसे अपने वशमें
कर ही लेना चाहिये। पापियोंके साथ
कभी मेल नहीं करना चाहिये।
अपने राज्य (राष्ट्र) को बाजारका
सौदा नहीं बनाना चाहिये।।”
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २३३