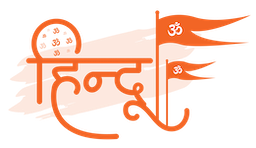राजनीतिकी विश्वस्तरपर सर्वसम्मत परिभाषा

“सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सम्पन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाजकी संरचना राजनीतिकी मन्वादि धर्मशास्त्रसम्मत विश्वस्तरपर सर्वसम्मत सार्वभौम परिभाषा है।”
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “सूक्तिसुधा” (सूक्तिशतक) पृष्ठ संख्या ३२
धर्म और नीति

‘धृञ् – धारणे’ धातु से ‘धर्म’ और ‘णीञ् प्रापणे’ धातु से ‘नीति’ शब्द सिद्ध होता है — ‘ध्रियतेऽभ्युदयोऽनेनेति धर्म:’, ‘नीयते प्राप्यतेऽभ्युदयोऽनयेति नीति:’।
अर्थात् अभ्युदयका धारण जिससे हो, वही ‘धर्म’ और अभ्युदयकी प्राप्ति जिससे हो, वही ‘नीति’ है।
फलतः दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसलिए कुछ लोग तो नीति को ही धर्म कहते हैं। पर कुछ लोग लौकिक अभ्युदय (उन्नति) के साधन को ‘नीति’ और पारलौकिक उन्नति के साधन को ‘धर्म’ कहते हैं। यह विभाग भी प्रधानता और अप्रधानता की ही दृष्टि से है। धर्म से पारलौकिक उन्नति प्रधानरूप से और गौणरूप से लौकिक उन्नति भी होती है। इसी तरह नीति से लौकिक उन्नति प्रधानरूप से और अप्रधानरूप से पारलौकिक उन्नति भी होती है।
धर्म और नीति का परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। नीति से ही शास्त्र और धर्म प्रतिष्ठित होते हैं, नीति के बिना शास्त्र और धर्म नष्ट हो जाते हैं —— ‘नश्येत् त्रयी दण्डनीतौ हतायाम्’। नीति से ही सामाजिक सुव्यवस्था, शान्ति होने पर धर्म के अनुष्ठान में सुविधा होती है और धर्म – भावना फैलने से ही नीति भी कार्य्यान्वित एवम् सफल होती है। अहिंसा और सत्य की भावना से राजा – प्रजा, मजदूर – पूँजीपति सभी में सद्भावना फैलती है। धर्म – भावना से ही परोक्ष में भी राजा – प्रजा अन्याय, अत्याचार से बचने का प्रयत्न करते हैं।
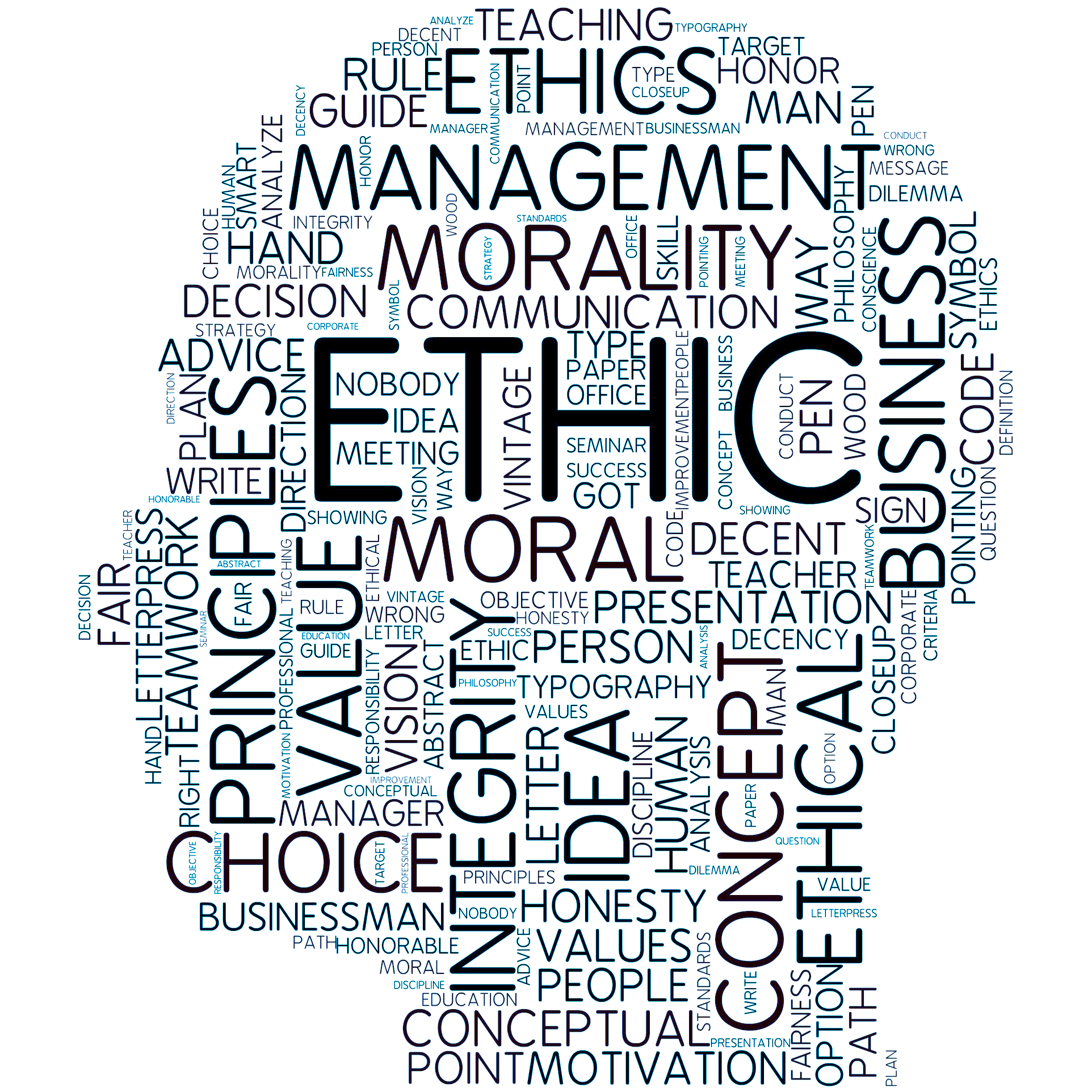
वास्तव में धर्म नीति का पति है। उससे विरहित होकर नीति विधवा है। बिना धर्मरूप पति के विधवा नीति पुत्रोत्पादन नहीं कर सकती। उसमें फलोत्पादन की क्षमता नहीं रहती। वैधव्य में वह केवल बिलबिलाती है, असफल होकर विलाप करती है। धर्मविरुद्ध नीति कहीं तत्काल अभ्युदय का साधन होती हुई भी परिणाम में अहितकारी सिद्ध होती है। दुष्परिणाम – शून्य वास्तविक अभ्युदय के साधन को ही नीति कहा जा सकता है। जो परिणाम में अनिष्टकर हो, वह सच्चा अभ्युदय नहीं, केवल अभ्युदयाभास है, अतः उसका साधन भी नीति नहीं केवल नीत्याभास है।
अर्थानुबन्ध, धर्मसम्बन्ध अभ्युदय ही सच्चा अभ्युदय है। अनर्थानुबन्ध, अधर्मानुबन्ध या अननुबन्ध अभ्युदय देखने भर को अभ्युदय है। विष से मिला हुआ मधुर पक्वान्न सेवन में तात्कालिक आनन्द देनेवाला होने पर भी मृत्यु का कारण होता है, यह स्पष्ट ही है। धर्मविहीन नीति आरम्भ में भले ही चामत्कारिक सफलता दिखलाये पर अन्त में वह पतन की ओर ही ले जायगी। समस्त ‘महाभारत’ इसका ज्वलन्त उदाहरण है। धर्मविरुद्ध साम्राज्य का उपभोग मिल गया, पर अन्त में पूर्ण पतन ही हुआ। धर्मनीति के अनुयायी बनकर युधिष्ठिर को १४ वर्ष वनों में भटकना पड़ा, पर अन्त में साम्राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ। इतिहास, पुराणों में सर्वत्र यही दिखलाया गया है कि ‘यतो धर्मस्ततो जय:’।

अपने यहाँ नीति साहित्य की कमी नहीं है। शुक्र, कौटिल्य, कामन्दक आदि की नीति के सामने पाश्चात्य नीति तुच्छ जँचती है। कहा तो यह जाता है कि नाजियों ने बहुत कुछ अर्थशास्त्र से सीखा है। कूटनीति के ऐसे दावपेंच बतलाये गये हैं, जिन्हें देखकर हैरान होना पड़ता है। यदि तुलना की जाय तो पाश्चात्य कूटनीति के प्रसिद्ध आचार्य मैकेवली को कौटिल्य के आगे सिर झुकाना पड़ेगा। परन्तु भेद इतना ही है कि हमारे यहाँ के नीतिज्ञों ने कभी भी धर्म को नहीं भुलाया। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है — ‘संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकम् । यस्मिन्नथें विरुध्येत धर्मेणार्थं विनिश्चयेत् ।’ ‘सर्वधर्म: स्वर्गायानन्त्याय च । तस्यातिक्रमे लोक: सङ्करादुच्छिद्येत ।’
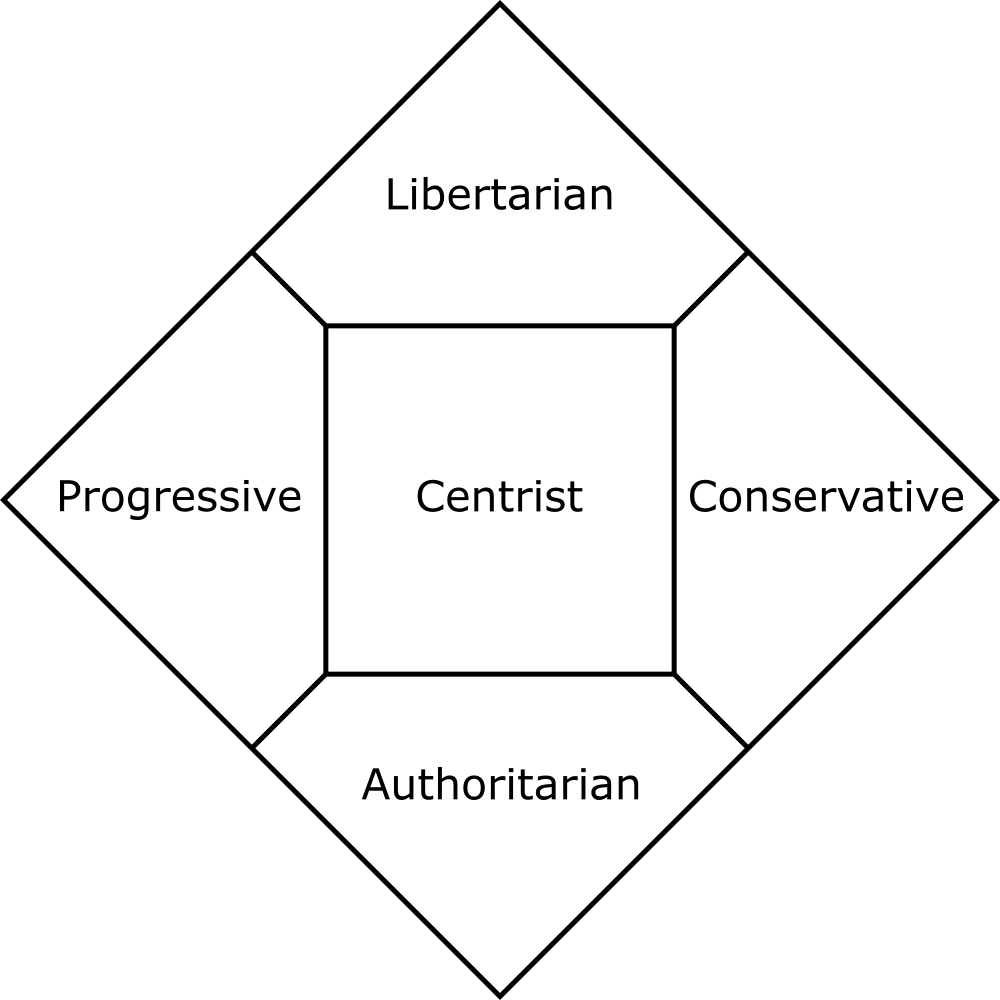
परन्तु इसका ध्यान न रखने का भी फल यह होता है कि आज पचासों वर्ष का हमारा प्रयत्न विफल रहा है। हमारी कोई भी नीति कारगर नहीं हो रही है। जो कुछ भी हम करते हैं, उसका फल उलटा ही होता है। आज के बड़े – बड़े नेता जिस नीति का आश्रय लेकर देश को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, वह भारत की नीति नहीं है। वास्तव में तो हम पाश्चात्य उच्छिष्ट नीति के अनुसरण में ही सारा जोर लगा रहे हैं। अपने प्राचीन नीति – साहित्य की ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता है। यदि उसे अपनायें तो फिर धर्म – विमुखता भी न रहे और धर्म का आश्रय लेने पर सफलता बनी बनायी है। धर्मविमुख होकर आज सारा विश्व पतन की ओर बढ़ रहा है, तरह – तरह के “वादों” के बादल छाये हुए हैं, उनमें से जीवन प्रदान करनेवाले जल की एक बूँद नहीं टपकती, होती है केवल घोर गर्जना और पत्थरों तथा बिजली की मार।
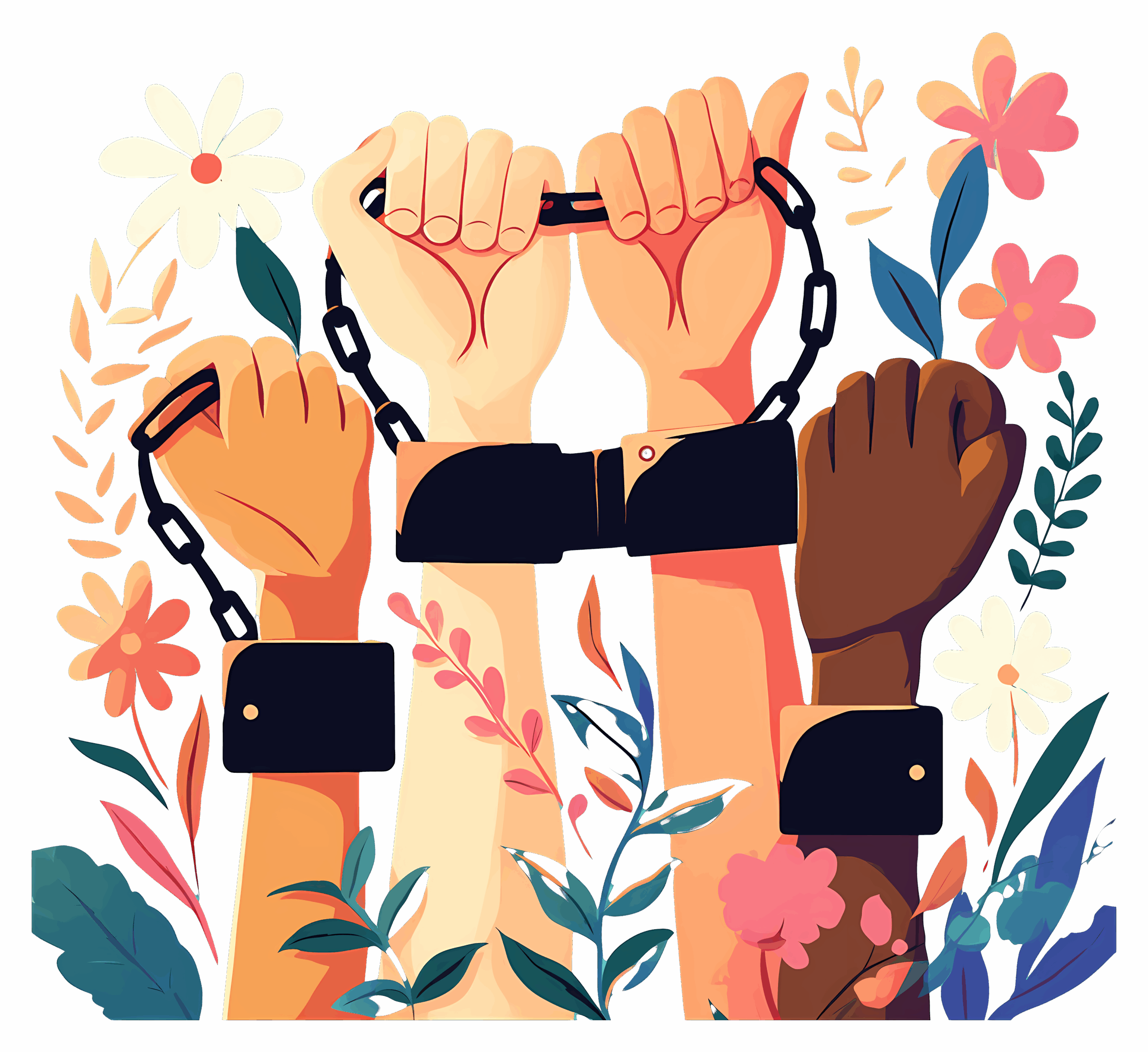
हम तो आज सब तरह से असमर्थ हैं। बाहुबल नहीं, शक्ति बल नहीं, बुद्धिबल नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी दशा में हम कर ही क्या सकते हैं ? हाँ, एक मार्ग हमारे सामने अवश्य है और वह है सर्व शक्तिमान् का सहारा। जितने भी आज हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, उनके साथ यदि हम भगवान् की प्रार्थना जोड़ दें तो हमारा मार्ग स्वतः साफ हो जायगा। उससे हमारा ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण होगा। भारत के महापुरुषों का यह आदर्श सिद्धान्त रहा है कि “सर्वे भवन्तु सुखिन:” । इसी दृष्टि से सदा उनकी प्रार्थना होती रही है। आज भी इसी की आवश्यकता है। यदि नियमपूर्वक इसके लिए प्रयत्न किया जाय तो सफलता अवश्यम्भावी है।
— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित
पुस्तक “करपात्र चिन्तनम्” पृष्ठ संख्या ३४ – ३७
(सिद्धान्त, वर्ष २, अंक ४२)
भारतीय राजनीतिशास्त्र
आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्।
तत: पुत्रांस्ततोऽमात्यान् ततो भृत्यान् तत: प्रजा:।।
(शुक्रनीति १. ९२)

— धर्मसम्राट् पूज्य स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज द्वारा लिखित
पुस्तक “मार्क्सवाद और रामराज्य” पृष्ठ संख्या ११२७
कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठ:
कालेनान्यस्तस्य मूलं हरेत कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठ:।।
(महाभारत – शान्तिपर्व १२०. ३९)

“शत्रु बाल, युवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, सदा सावधान न रहनेवाले मनुष्यका नाश कर डालता है। अन्य कोई धनसम्पन्न शत्रु अनुकूल समयका सहयोग पाकर राजाकी जड़ उखाड़ सकता है। अत एव जो समयको जानता है, वही राजाओं में श्रेष्ठ है।।“
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २३०
षड्गुण
सन्धिश्च विग्रहश्चैव यानमासनमेव च।
द्वैधीभाव: संश्रयश्च षड्गुणा: परिकीर्त्तिता:।।
(महाभारत – शान्तिपर्व २३४. १७)
“किसी शर्तपर समकक्ष या प्रबल शत्रुसे सामञ्जस्य ‘सन्धि’ है। युद्धादिके द्वारा उसे हानि पहुँचाना ‘विग्रह’ है। विजयाभिलाषी राजा जो शत्रुके ऊपर चढ़ाई करता है, वह यात्रा या ‘यान’ है। विग्रह छेड़कर अपने ही देशमें रहना ‘आसन’ है। आधी सेनाको किलेमें छिपाकर आधी सेनाके साथ युद्धकी भावनासे यात्रा करना ‘द्वैधीभाव’ है। असमर्थताकी दशामें लाभकी सम्भावना होने पर उदासीन अथवा मध्यम राजाकी शरणागति ‘संश्रय’ है।“
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २२८
बुद्धे: पश्चात् कर्म यत्तत् प्रशस्तम्
प्रत्यक्षेणानुमानेन तथौपम्यागमैरपि।
परीक्ष्यास्ते महाराज स्वे परे चैव नित्यश:।।
(महाभारत — शान्तिपर्व ५६. ४१)
“महाराज ! प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम — इन चारों प्रमाणोंके द्वारा सदा अपने – परायेकी पहचान करते रहना चाहिये।।”
प्रत्यक्षनुमानं च सर्वेषां योनिरिष्यते।
प्रमाणज्ञो हि शक्नोति दण्डनीतौ विचक्षण:।।
अप्रमाणवतां नीतो दण्डो हन्यान्महीपतिम्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २४. दा०)
“इनमेंसे प्रत्यक्ष और अनुमान — ये दो सबके लिये निर्णयके आधार माने गये हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणोंको जाननेवाला पुरुष दण्डनीतिमें कुशल हो सकता है। जो प्रमाणशून्य हैं, उनके द्वारा प्रयोगमें लाया गया दण्ड राजाका विनाश कर सकता है।।”

तर्कशास्त्रकृता बुद्धिर्धर्मशास्त्रकृता च या।
दण्डनीतिकृता चैव त्रैलोक्यमपि साधयेत्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २४. दा०)
“तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दण्डनीतिसे परिष्कृत — बुद्धि तीनों लोकोंकी भी सिद्धि कर सकती है।।”
आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतिषु पारगा:।
ते तु सर्वत्र योक्तव्यास्ते च बुद्धे: परं गता:।
गुणयुक्त्तेऽपि नैकस्मिन् विश्वसेत विचक्षण:।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २४. १८)
“आन्विक्षिकी (वेदान्त), वेदत्रयी, वार्ता तथा दण्डनीतिके जो पारङ्गत विद्वान् हों, उन्हें सब कार्योंमें नियुक्त करना चाहिये; क्योंकि वे बुद्धिकी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए होते हैं। एक व्यक्ति कितना ही गुणवान् क्यों न हों, विद्वान् पुरुषको केवल उसपर विश्वास कर उसीके भरोसे नहीं रहना चाहिये।।”
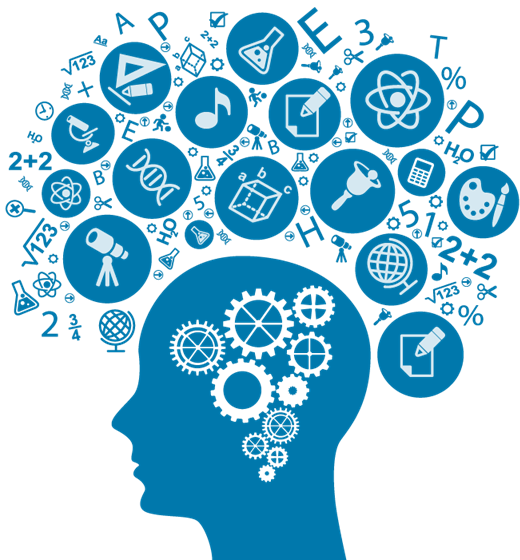
बुद्धिर्दीप्ता बलवन्तं हिनस्ति बलं बुद्ध्या पाल्यते वर्धमानम्।
शत्रुर्बुद्ध्या सीदते वर्धमानॊ बुद्धेः पश्चात् कर्म यत्तत् प्रशस्तम्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व १२०. ४२)
“प्रतिभाशालिनी बुद्धि बलवान् को भी पछाड़ देती है। बुद्धिके द्वारा नष्ट होते हुए बलकी भी रक्षा होती है। बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धिके द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है। बुद्धिसे सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है, वह सर्वोत्तम है।।”
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २२२-२२४
विपत्तिस्थस्य राज्ञः कर्तव्यानां वर्णनम्
परचक्राभियातस्य दुर्बलस्य बलीयसा।
आपन्नचेतसॊ ब्रूहि किं कार्यमवशिष्यते।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ३)
“जिसपर शत्रुदलका आक्रमण हो गया हो, जो दुर्बल होकर बलवान शत्रुके द्वारा पीड़ित हो और विपत्तिमें पड़कर जिसका चित्त घबरा उठा हो, उसके लिये कौन-सा कार्य शेष रह जाता है? — उसे इस संकटसे मुक्त होनेके लिये क्या करना चाहिये? ।।”
बाह्यश्चेद् विजिगीषुः स्याद् धर्मार्थकुशलः शुचिः।
जवेन संधिं कुर्वीत पूर्वभुक्तान् विमॊचयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ४)
“राजन ! यदि विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाला राजा बाहरका हो, उसका आचार-विचार शुद्ध हो तथा वह धर्म और अर्थके साधनमें कुशल हो तो शीघ्रतापूर्वक उसके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये और जो ग्राम तथा नगर अपने पूर्वजोंके धिकारमें रहे हों, वे यदि आक्रमणकारीके हाथमें चले गये हों तो उसे मधुर वचनोंद्वारा समझा-बुझाकर उसके हाथसे छुड़ानेकी चेष्टा करे।।”

योऽधर्मविजिगीशु: स्याद् बलवान् पापनिश्चयः।
आत्मनः संनिरॊधेन संधिं तेनापि रोचयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ५)
“जो विजय चाहनेवाला शत्रु अधर्मपरायण हो तथा बलवान होनेके साथ ही पापपूर्ण विचार रखता हो, उसके साथ अपना कुछ खोकर भी सन्धि कर लेनेकी ही इच्छा रखे।।”
अपास्य राजधानीं वा तरेद् द्रव्येण चापदम्।
तद्भावयुक्तो द्रव्याणि जीवन् पुनरुपार्जयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ६)
“अथवा आवश्यकता हो तो अपनी राजधानीको भी छोड़कर बहुत-सा द्रव्य देकर उस विपत्तिसे पार हो जाय। यदि वह जीवित रहे तो राजोचित गुणसे युक्त होनेपर पुनः धनका उपार्जन कर सकता है।।”

अवरॊधान् जुगुप्सेत का सपत्नधने दया।
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथंचन।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ८)
“शत्रुका आक्रमण हो जानेपर राजाको सबसे पहले अपने अन्तःपुरकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये। यदि वहाँ शत्रुका अधिकार हो जाय, तब उधरसे अपनी मोह-ममता हटा लेनी चाहिये; क्योंकि शत्रुके अधिकारमें गये हुए धन और परिवारपर दया दिखाना किस कामका? जहाँतक सम्भव हो, अपने-आपको किसी तरह भी शत्रुके हाथमें नहीं फँसने देना चाहिये।।”
आभ्यन्तरे प्रकुपिते बाह्ये चॊपनिपीडिते।
क्षीणे कॊशे श्रुते मन्त्रे किं कार्यमवशिष्यते।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ९)
“पितामह! यदि बाहर राष्ट्र और दुर्ग आदिपर आक्रमण करके शत्रु उसे पीड़ा दे रहे हों और भीतर मन्त्री आदि भी कुपित हों, खजाना खाली हो गया हो और राजाका गुप्त रहस्य सबके कानोंमें पड़ गया हो, तब उसे क्या करना चाहिये? ।।”

क्षिप्रं वा संधिकामः स्यात् क्षिप्रं वा तीक्ष्णविक्रमः।
तदापनयनं क्षिप्रमेतावत् साम्परायिकम्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १०)
“राजन्! उस अवस्थामें राजा या तो शीघ्र ही सन्धिका विचार कर ले अथवा जल्दी-से-जल्दी दुःसह पराक्रम प्रकट करके शत्रुको राज्यसे निकाल बाहर करे, ऐसा उद्योग करते समय यदि कदाचित् मृत्यु भी हो जाय तो वह परलोकमें मंगलकारी होती है।।”
अनुरक्तेन चेष्टेन हृष्टेन जगतीपति:।
अल्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति भूमिप:।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. ११)
“यदि सेना स्वामीके प्रति अनुराग रखनेवाली, प्रिय और हृष्ट-पुष्ट हो तो उस थोड़ी-सी सेनाके द्वारा भी राजा पृथ्वीपर विजय पा सकता है।।”

हतॊ वा दिवमारॊहेद्धत्वा वा क्षितिमावसेत्।
युद्धे हि संत्यजन् प्राणान् शक्रस्यैति सलॊकताम्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १२)
“यदि वह युद्धमें मारा जाय तो स्वर्गलोकके शिखरपर आरूढ़ हो सकता है अथवा यदि उसीने शत्रुको मार लिया तो वह पृथ्वीका राज्य भोग सकता है। जो युद्धमें प्राणोंका परित्याग करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है।।”
सर्वलॊकागमं कृत्वा मृदुत्वं गन्तुमेव च।
विश्वासाद् विनयं कुर्याद् विश्वसेच्चाप्युपायत:।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १३)
“अथवा दुर्बल राजा शत्रुमें कोमलता लानेके लिये विपक्षके सभी लोगोंको संतुष्ट करके उनके मनमें विश्वास जमाकर उनसे युद्ध बंद करनेके लिये अनुनय-विनय करे और स्वयं भी उपायपूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे।।”

अपचिक्रमिषु: क्षिप्रं साम्ना वा परिसान्त्वयन्।
विलङ्घयित्वा मन्त्रेण ततः स्वयमुपक्रमेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व १३१. १४)
“अथवा वह मधुर वचनोंद्वारा विरोधी दलके मन्त्री आदिको प्रसन्न करके दुर्गसे पलायन करनेका प्रयत्न करे। तदनन्तर कुछ काल व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति ले अपनी खोयी हुई सम्पत्ति अथवा राज्यको पुनः प्राप्त करनेका प्रयत्न आरम्भ करे।।”
(महाभारत – शान्तिपर्व १३१-वाँ अध्याय)
राज्यं पण्यं न कारयेत्
तरसा बुद्धिपूर्वं वा निग्राह्या एव शत्रव:।
पापै: सह न संदध्याद् राज्यं पण्यं न कारयेत्।।
(महाभारत-शान्तिपर्व २४. १६)
“शत्रुओंको बल
और बुद्धिसे अपने वशमें
कर ही लेना चाहिये। पापियोंके साथ
कभी मेल नहीं करना चाहिये।
अपने राज्य (राष्ट्र) को बाजारका
सौदा नहीं बनाना चाहिये।।”
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या २३३