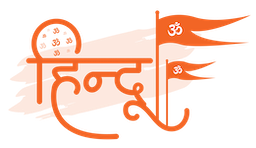(सनातनधर्म की चौबीस विशेषताएँ)
सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वर धर्म
प्रश्न उठता है कि यदि सर्वधर्मोंका गन्तव्य एक ही है, सबका आदर्श एक ही है, तब सनातनधर्मके अतिरिक्त धर्म, मत, पन्थ या मजहब कुछ काल तक ही किसी व्यक्ति, वर्ग और क्षेत्रविशेषको प्रभावितकर विलुप्त क्यों हो जाते हैं?

उत्तर स्पष्ट है कि सनातनधर्ममें सन्निहित समस्त दिव्यताओंके समादरके अभावके कारण विविध वादों, पन्थों और तन्त्रोंका किञ्चित् उत्कर्षके बाद पतन सम्भावित और सुनिश्चित है। वस्तुतः क्रिश्चियन रिलिजन, मुसलिम मजहबको उनकी दृष्टिसे धर्म मानना भी अनुचित है।
‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’ (वैशेषिकदर्शन १. २) के अनुसार जिससे लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्ष हो; तद्वत् मोक्षसंज्ञक निःश्रेयससिद्धिमें हेतुभूत आत्मज्ञान हो, वह अभ्युदय है। अतः मानवधर्म, वर्णधर्म तथा आश्रमधर्मके सदृश ही मोक्ष भी धर्म मान्य है। यह तथ्य महाभारत तथा श्रीमद्भागवतादि आर्ष ग्रन्थोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। ‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ (पूर्वमीमांसा १. १. २) के अनुसार वेदविहित प्रयोजनकी सिद्धिमें हेतुभूत अनुष्ठेय यज्ञादिका नाम धर्म है। ‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ (पूर्वमीमांसा १. १. २) में प्रयुक्त ‘अर्थः’ का विवरण ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’ (वैशेषिकदर्शन १. १. २) में प्रयुक्त ‘अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः’ है तथा ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’ (वैशेषिकदर्शन १. १. २) में प्रयुक्त ‘यतः’ का विवरण ‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ (पूर्वमीमांसा १. १. २) में प्रयुक्त ‘चोदनालक्षणः’ (पूर्वमीमांसा १. १. २) है।
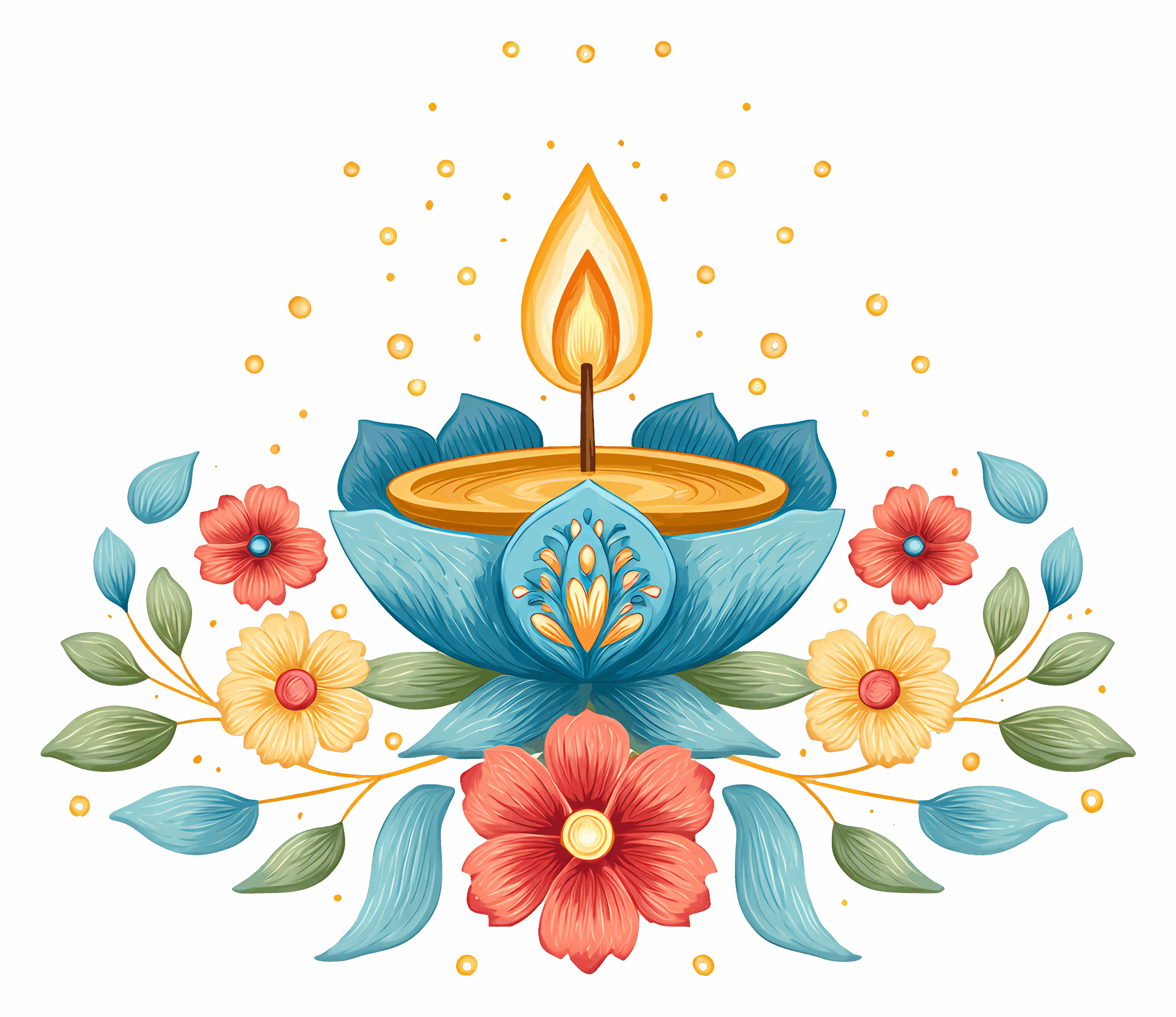
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षसंज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टयमें परिगणित धर्म चित्तशोधक यज्ञादि कर्म एवम् श्रद्धादि शुद्ध मनोभावका द्योतक है; अत एव वह स्थावर – जङ्गम प्राणियोंके सहित पृथ्वीका धारक और पोषक है। —
धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च।
अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः।।
(महाभारत — अनुशासनपर्व १५०. ४१)
“धर्म, काम, अर्थसाधक वसु और वासुकि, मोक्षप्रदायक अनन्त तथा कपिल एवम् पुरुषार्थ चतुष्टयकी सिद्धिमें हेतुभूत काल – ये सात पृथ्वीके धारक हैं।।”
धर्मेति धारणे धातुर्माहात्म्ये चैव पठ्यते।
धारणाच्च महत्त्वेन धर्म एष निरुच्यते।।
(मत्स्यपुराण १३४. १७)
“धृ – धातु धारण – पोषण और महत्त्वके अर्थमें प्रयुक्त होती है। इसी धातुसे ‘धर्म‘ शब्द निष्पन्न हुआ है। महत्त्वशील और धारक होनेसे यह धर्म – ‘धर्म‘ कहा जाता है।।”
धारणाद् धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः।
य: स्याद् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः।।
(महाभारत — शान्तिपर्व १०९. ११)
“धर्म धारण करता है, अर्थात् अस्तित्व और आदर्शकी रक्षाकर अधोगतिसे बचाता है, इसलिए उसे धर्म कहा गया है। धर्मने ही सारी प्रजाको धारण कर रक्खा है। अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो, वही धर्म है, ऐसा सत्पुरुषोंका निश्चय है।।”

सनातन वैदिक धर्म
धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।
यत् स्यात् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः।।
(महाभारत — कर्णपर्व ६९. ५८)
“धर्म ही प्रजाको धारण करता है और धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं। अत एव जो धारण – प्राणरक्षाके युक्त हो, जिसमें किसी जीवका उत्पीडन – शोषण – अहित न हो, वह धर्म है, ऐसा शास्त्रोंका सिद्धान्त है।।”
अकारणो हि नैवास्ति धर्मः सूक्ष्मो हि जाजले।
भूतभव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २६२. ३५)
“जाजले ! कोई भी धर्म निष्प्रयोजन या निष्फल नहीं है। उसका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। भूत संज्ञक सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म और स्वर्गादिसाधक भव्यसंज्ञक अनुष्ठेय यज्ञादिकी सिद्धिके लिए ही धर्मका प्रवचन किया गया है।।”
पृथिवीसे पुरुषपर्यन्त साङ्ख्यसम्मत पचीस सिद्ध वस्तुओंका नाम भूत है।—
पुरुषः प्रकृतिर्बुद्धिर्विषयाश्चेन्द्रियाणि च।
अहङ्कारोऽभिमानश्च समूहो भूतसंज्ञकः।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २०५. २४)
अभिप्राय यह है कि पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्वात्मिका बुद्धि, अहङ्कार, मन, शब्दादि पञ्च तन्मात्रात्मक अपञ्चीकृत पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय तथा पञ्च स्थूल भूत संज्ञक पचीस तत्त्वकी भूत संज्ञा है।

अनुष्ठेय यज्ञादि शोधक क्रिया एवम् श्रद्धादि शुद्ध मनोभावका नाम भव्य है। यज्ञादि भव्य और ब्रह्म तथा ब्रह्माधिष्ठिता प्रकृतिसे समुद्भूत आकाशादि भूत धारक होनेके कारण धर्म हैं।
शमो दमस्तथा धैर्यं सत्यं शौचमथार्जवम्।
यज्ञो धृतिश्च धर्मश्च नित्यमार्षो विधिः स्मृतः।।
(महाभारत — शान्तिपर्व १२. १७)
“शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ, धृति तथा आत्मज्ञानरूप धर्मके निरन्तर सेवनकी आर्षविधि है। इनके परिपालनसे ऋषियोंकी प्रसन्नता सुनिश्चित है।।”
उक्त रीतिसे वेदादि शास्त्रसम्मत सर्वधारक – पोषक – प्रकाशक तथा आह्लादक यज्ञादि कर्म, श्रद्धादि मनोभाव तथा सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वर धर्म है।
पृथिवीमें गन्ध, जलमें रस, तेजमें रूप, वायुमें स्पर्श, आकाशमें शब्दके सदृश विश्वमें सन्निहित सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरकी सर्वधारकता, पोषकता, प्रकाशकता तथा आह्लादकता समुद्धृत वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। —
‘पुण्यो गन्धः पृथिव्यां’ (गीता ७. ९), ‘रसोऽहमप्सु’ (गीता ७. ८), ‘तेजश्चास्मि विभावसौ’ (गीता ७. ९), ‘पवनः पवतामस्मि’ (गीता १०. ३१), ‘शब्दः खे’ (गीता ७. ८), ‘गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।।’ (गीता १५. १३), ‘अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।।’ (गीता १३. १४), ‘यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्।।’ (गीता १५. १२), ‘द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधेः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः।।’ (महाभारत – अनुशासनपर्व १४९. १३४) के अनुसार पृथ्वीमें पुण्य गन्ध, जलमें रस, अग्निमें तेज, पवनमें पवित्रता, आकाशमें शब्द – मूलक अस्तित्व और उपयोगिताके ख्यापक तथा दिशा, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रसहित त्रिभुवनके विधारक, परिपोषक और आह्लादक सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वर हैं।
जीवात्मतत्त्वकी धारकता; अत एव धर्मरूपता समुद्धृत वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। —
‘इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्।।’ (गीता ७. ५), ‘एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तानेवानुविधावति’ (कठोपनिषत् २.४.१४)
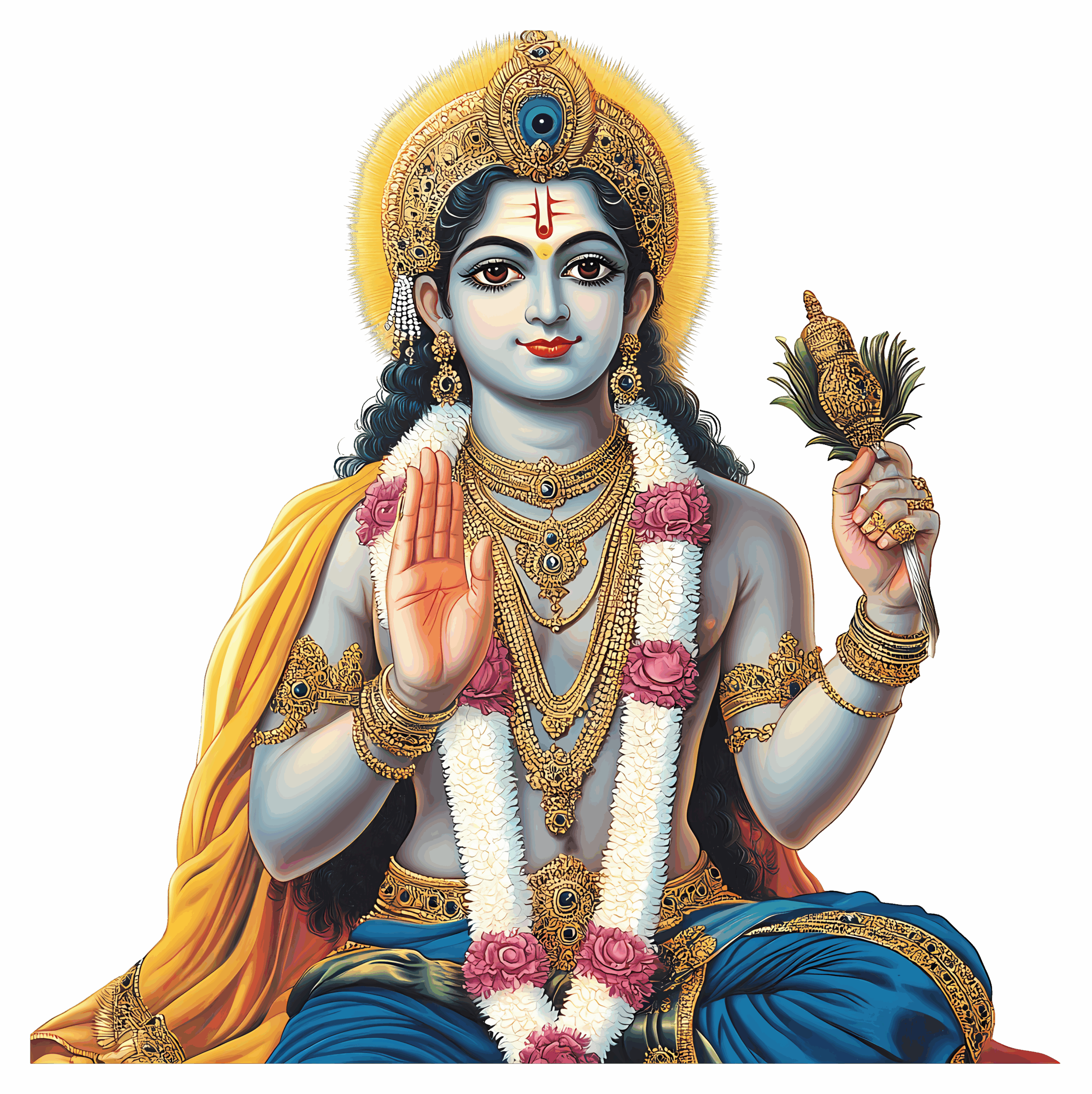
वस्तुस्थिति यह है कि “न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति” (श्रीमद्भागवत ५. ११. १) – “विचारकुशल मनीषिगण व्यावहारिक मान्यताओंको ताकपर रखकर ही तत्त्वविचार करते हैं।।”, “परावरदृशः शक्तिर्ज्ञानमूला न नश्यति” (महाभारत – शान्तिपर्व ३२९. ५१) – “सर्वात्मदर्शी तत्त्वज्ञकी ज्ञानात्मिका शक्ति कभी नष्ट नहीं होती; अर्थात् सदा तत्त्वदर्शनशीला होती है”, “परावरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिम्” (महाभारत – अनुशासनपर्व १५१. १२) – “परम तत्त्वके विशेषज्ञकी परम तत्त्वतक गति सुनिश्चित है”, “गतिज्ञाः सर्वभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः” (महाभारत – अनुशासनपर्व १५१. ११) – “अध्यात्मगति परमतत्त्वके चिन्तक समस्त प्राणियोंकी गतिके मर्मज्ञ होते हैं; अर्थात् परमतत्त्व सबका गन्तव्य है, उन्हें इस तथ्यका ज्ञान होता है।”, “तत्त्वपक्षपातो हि स्वभावो धियाम्” – ‘तथ्यात्मक तत्त्वका पक्षधर होना बुद्धि (जीव) का स्वभाव है’ (बौद्धागमसिद्धान्त) इन सूक्तियोंमें आस्थान्वित रहते हुए उक्त प्रश्नका उत्तर हृदयङ्गम करने योग्य है।
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या ५०५ – ५०९
सनातनधर्ममें लक्ष्य – पुरुषार्थचतुष्टयके
माध्यमसे भोग और मोक्ष
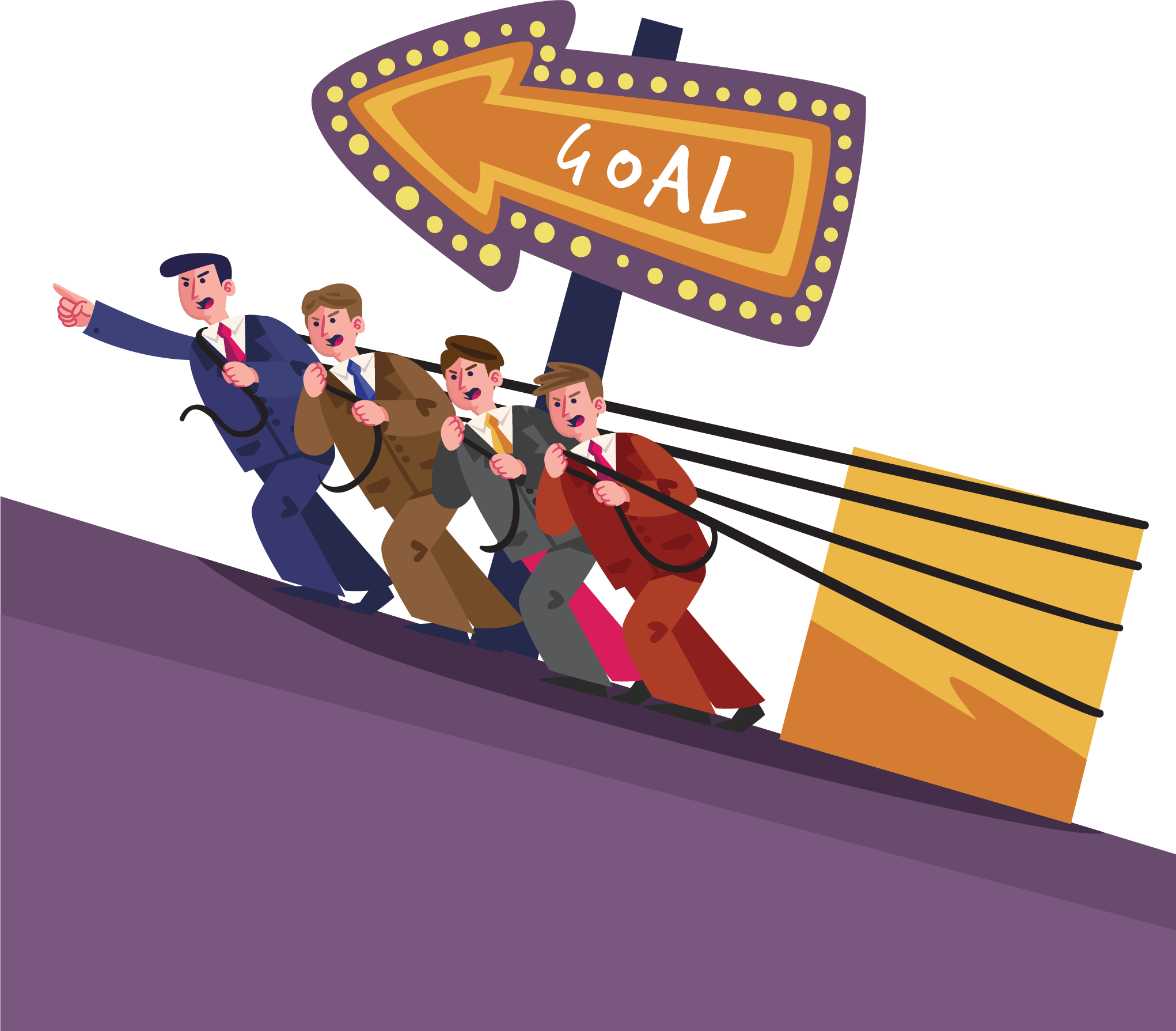
(१) पहली विशेषता — सनातनधर्ममें लक्ष्यका निर्धारण सुस्पष्ट है। इसके अनुसार प्रलयोत्तर महासर्गके प्रारम्भमें सर्वेश्वर जीवोंके देह, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणसे युक्त जीवनकी तथा बाह्य जगत् की संरचना इस अभिप्रायसे करते हैं कि पूर्व कल्पोंमें अकृतार्थ प्राणी पुरुषार्थचतुष्टयके माध्यमसे भोग और मोक्ष सुलभ कर सकें। —
बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् जनानामसृजत्प्रभुः।
मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च।।
(श्रीमद्भागवत १०. ८७. २)
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थचतुष्टय हैं। भोग्यसामग्रीका नाम अर्थ है । भोग्य सामग्रीके उपभोगका नाम काम है। अर्थोपार्जन और विषयोपभोगकी भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल विधाका नाम धर्म है। मृत्यु, मोह, दुःख, परतन्त्रता और अनियामकताकी आत्यन्तिकी निवृत्ति और स्वतन्त्रता तथा प्रभुतासम्पन्न सच्चिदानन्दरूपताकी समुपलब्धि मुक्ति या मोक्ष है।
दुःखका हेतु जन्म है। जन्मका हेतु धर्माधर्मरूप प्रवृत्ति है। प्रर्वत्तका मूल राग – द्वेषरूप दोष है। दोषका बीज मिथ्याज्ञान है। जैसे कफके निवारणसे कफसे उद्भूत ज्वरका निवारण सम्भव है, वैसे ही जन्मके निवारणसे दुःखका, धर्माधर्मके निवारणसे जन्मका, राग द्वेषके निवारणसे धर्माधर्मरूप प्रवृत्तिका और मिथ्याज्ञानके निवारणसे रागद्वेषरूप दोषका निवारण सुनिश्चित है – “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्या-ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:” (न्यायदर्शन १. १. २)
वेदान्तप्रस्थानके अनुसार मिथ्याज्ञान अविद्या है। वही दुःखदोषका परम कारण है। अविद्यानिवृत्तिसे ब्रह्मरूपाविर्भाव मोक्ष है।
“अविद्यानिवृत्त्या ब्रह्मरूपाविर्भावो मोक्षः” (भामती १. १. ४)

धर्मशास्त्रोंके अनुशीलनसे अद्भुत प्रज्ञाका उदय होता है। देहसे अतिरिक्त तथा अतीत नित्य और चेतन आत्माके अस्तित्वमें आस्था धर्मानुष्ठानका मूल है। देहके भेदसे आत्मभेद और देहके नाशसे आत्मनाश असिद्ध है। विविध स्वप्नगत स्व तथा पर विविध शरीरोंके भेद तथा नाशसे आत्मभेद और नाश अमान्य है। धर्मानुष्ठानके लिए पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्ममें एवं उत्क्रमण और अधोगतिमें परम्पराप्राप्त आस्था और आगमिक युक्तियोंके बलपर विश्वास आवश्यक है। धर्मानुष्ठानसे जन्म, उत्क्रमण, अधोगतिरहित आत्मस्थितिरूपा मुक्तिके लिए अपेक्षित बल, वेग और अभिरुचिरूपा अधिकारसम्पदा सुलभ होती है। धर्मानुष्ठान और उसके लिये अपेक्षित संस्कारोंका मूल सनातन वर्णाश्रमव्यवस्था है।

संस्करणका नाम ‘संस्कार‘ है। ‘सम्‘ उपसर्गसे ‘कृञ्‘ धातुको ‘घञ्‘ प्रत्यय और ‘संपरिभ्यां करोतौ भूषणे‘ (पाणिनीय ६. १. १३७) सूत्रसे भूषण अर्थमें ‘सुट्‘ आगम करनेपर ‘संस्कार‘ शब्द बनता है। महर्षि जैमिनिप्रणीत ‘द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः‘ (३. १. १) सूत्रके भाष्यमें श्रीशबरपादमहाभागने संस्कारको परिभाषित करते हुए कहा है – ‘संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य‘ – ‘संस्कार वह होता है, जिसके उत्पन्न होनेपर पदार्थ किसी प्रयोजनके लिये योग्य होता है‘। तन्त्रवार्तिककार श्रीभट्टपादके अनुसार संस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं, जो योग्यता प्रदान करती हैं – ‘योग्यतां चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते‘।
मलापनयन, हीनाङ्गपूर्ति और अतिशयाधान – भेदसे संस्कार तीन प्रकारके होते हैं। विजातीय द्रव्यके योगसे मलिन सुवर्णको घर्षणादिके द्वारा निर्मल बनाना मलापनयन है। आभूषणके रूपमें स्थैर्य प्रदान करनेके लिए उसमें किञ्चित् ताम्रधातुका सन्निवेश हीनाङ्गपूर्ति है। उसे आभूषणका रूप प्रदानकर उसमें यथास्थान हीरा, मोती आदिका योग अतिशयाधान है।

वस्तुको भोग या अपवर्गके अनुरूप बनानेकी विधा संस्कार है। जगत् नाम (समाख्या), रूप, कर्मात्मक है। सनातन शास्त्रोंमें इन्हें संस्कृत करनेकी अपूर्व विधाका वर्णन है। देव, ऋषि, पितर और परमेश्वरके प्रसादका तथा दैवीसम्पत् का अभिव्यञ्जक कर्म तथा भाव संस्कार है। सत्ता, स्फूर्ति तथा सुखोपलब्धि उसका फल है। दोषापनयन तथा गुणाधानसे संस्कारकी सिद्धि होती है। मलिन दर्पणपर ईंटका चूर्ण रगड़नेसे दर्पण संस्कृत हो जाता है। यह दोषापनयनका उदाहरण है। बीजपूर (बिजौरी नीबू) आदिके फूलको लाखके रससे तर कर देनेपर उसका फल अन्दरसे लाल हो जाता है। यह गुणाधान संस्कार है। —
कुसुमे बीजपूरादेः यल्लाक्षाद्युपसिच्यते।
तदूपस्यैव सङ्क्रातिः फले तस्येति वासना।।
(प्रवाभा. पू. ३५८)
वैदिकसंस्कारसम्पन्न ब्राह्मणादि द्विज होते हैं। मन्त्रोंका विनियोग संस्कारोंमें होता है – ‘संस्कारेषु मन्त्रा विनियुज्यन्ते‘। इस मन्त्रसे यह संस्कार कर्त्तव्य है – ‘अनेन मन्त्रेणायं संस्कारः कर्त्तव्यः‘ – ऐसा बोध ब्राह्मणभागके द्वारा सम्भव है। इतिकर्त्तव्यता (सहायक व्यापार) का बोध सूत्रोंसे होता है- ‘सूत्रेणेतिकर्त्तव्यतोच्यते‘। सूत्रसे ब्राह्मणकी और ब्राह्मणसे मन्त्रकी सार्थकता सिद्ध होती है।
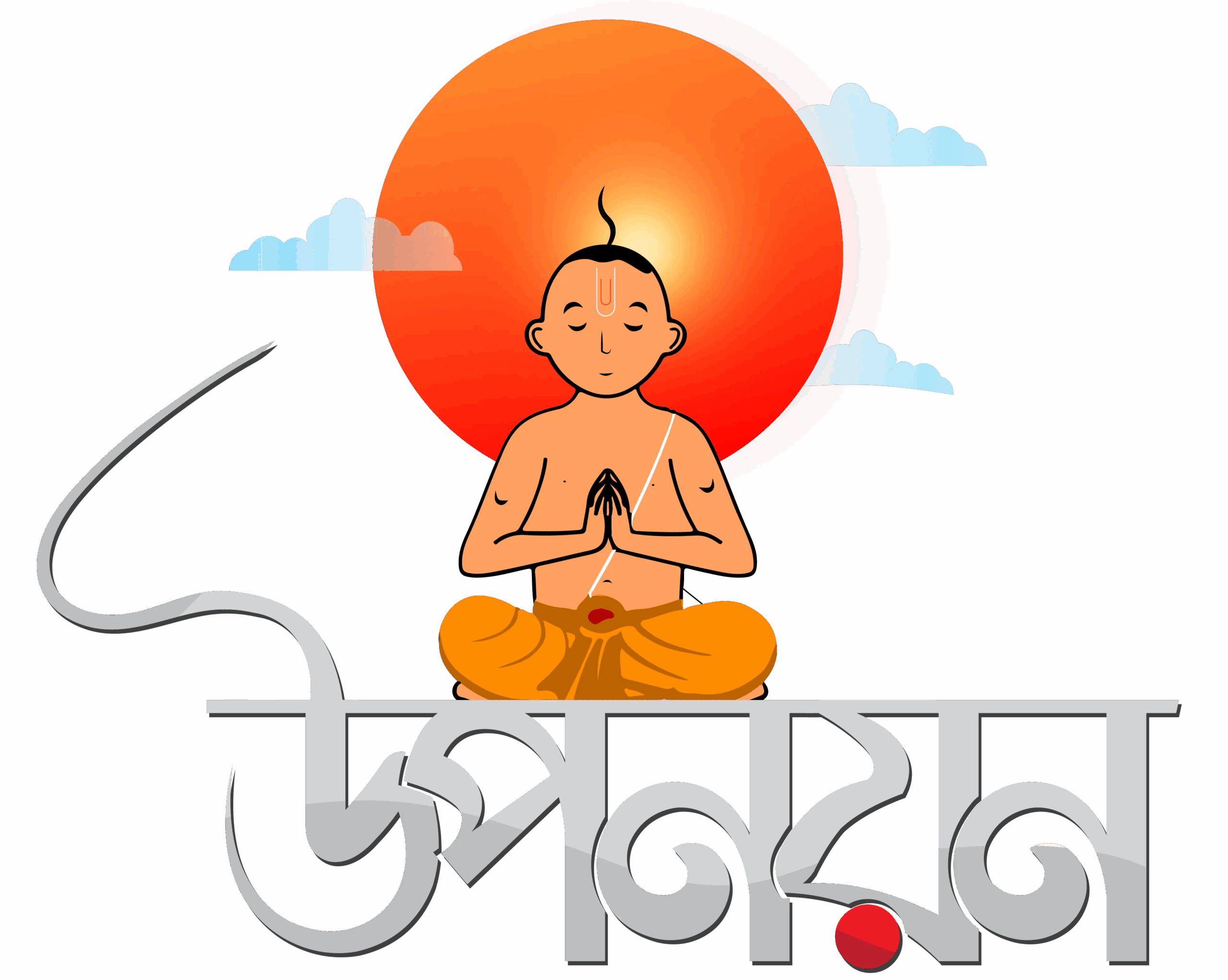
वैदिक संस्कारोंसे देह, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणका शोधन होता है। लौकिक तथा पारलौकिक अभ्युदय सुलभ होता है तथा निःश्रेयसरूप मोक्षका मार्ग प्रशस्त होता है। अत एव इस लोकमें तथा देहत्यागके पश्चात् परलोकमें सुखप्रद जीवनकी भावनासे ब्राह्मणादि वर्णोंका पवित्र संस्कार वेदोक्त मन्त्रोंसे अवश्य करना चाहिये। –
वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम्।
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च।।
(मनुस्मृति २. २६)
गर्भशुद्धिकारक हवन, जातकर्म, चूडाकरण (मुण्डन), मौजीबन्धन (उपनयन) – संस्कारोंसे द्विजोंके वीर्य तथा गर्भसे उत्पन्न दोष नष्ट होते हैं। —
गार्भैहोमैर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिबन्धनैः।
बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते।।
(मनुस्मृति २. २७)
महर्षि हारीतके अनुसार संस्कारोंकी ब्राह्म एवं दैव – संज्ञक दो श्रेणियाँ हैं। गर्भाधानादि स्मार्तसंस्कारोंको ब्राह्म कहते हैं। इनसे सम्पन्न ऋषिसदृश होकर ऋषिसायुज्य लाभ करते हैं। पाकयज्ञ (पकाये हुए भोजनकी आहुतियाँ), यज्ञ (होमाहुतियाँ) और सोमयज्ञादि दैवसंस्कार कहे जाते हैं। विधिवत् गर्भाधानसे पत्नीके गर्भमें भगवत्तत्त्वमें आस्थान्वित वेदार्थके अनुशीलनमें अभिरुचिसम्पन्न जीवका प्रवेश होता है। पुंसवनसंस्कारसे गर्भको पुरुषभावसे भावित किया जाता है। सीमोन्तोनयनके द्वारा माता पितासे उत्पन्न दोष दूर किया जाता है। बीज, रक्त तथा भ्रूणसे उत्पन्न दोष जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म और समावर्तनसे दूर होते हैं। इस प्रकार गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तोनयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण और समावर्तनसे पवित्रताका सम्पादन होता है। उपनयनादि अष्टविध संस्कारोंसे देव – पितृ – कार्योंमें परम पात्रता प्राप्त होती है। —

द्विविध एव संस्कारो भवति ब्राह्यो दैवश्च। गर्भाधानादिः स्नानान्तो ब्राह्मः। पाकयज्ञाः हविर्यज्ञाः सौम्याश्चेति दैवः। ब्राह्मसंस्कारसंस्कृतः ऋषीणां समानतां सलोकतां सायुज्यं गच्छति। गर्भाधानवदुपेतो ब्रह्मगर्भं संदधाति। पुंसवनात्पुंसी करोति। फलस्थापनान्मातापितृजं पाप्मानमपोहति। रेतोरक्तगर्भोपघातः पञ्चगुणो जातकर्मणा प्रथममपोहति। नामकरणेन द्वितीयं प्राशनेन तृतीयं चूडाकरणेन चतुर्थं स्नापनेन पञ्चममेतैरष्टाभिः संस्कारैर्गर्भोपघातात् पूतो भवतीति। उपनयनादिभिरष्टाभिरन्तर्वतै – श्चाष्टाभिः स्वच्छन्दैः सम्मिता ब्राह्मणाः परं पात्रं देवपितृणां भवन्ति। (संस्कारप्रकाश, संस्कारतत्त्व)
‘मनसा संस्करोति ब्रह्मा‘ (छान्दोग्योपनिषत् ४. १६. २) ‘ब्रह्मा यज्ञको मनसे सम्पन्न तथा संस्कृत करते हैं’ इस स्थलमें श्रुतिने संस्कृत शब्दका प्रयोग किया है। ‘चतुश्चत्वारिंशत्संस्कारसम्पन्नः‘ (नारदपरिव्राजकोपनिषत् १. १) इस कथनसे श्रुतिने चौवालीस संस्कारसम्पन्नताका उल्लेख किया है।
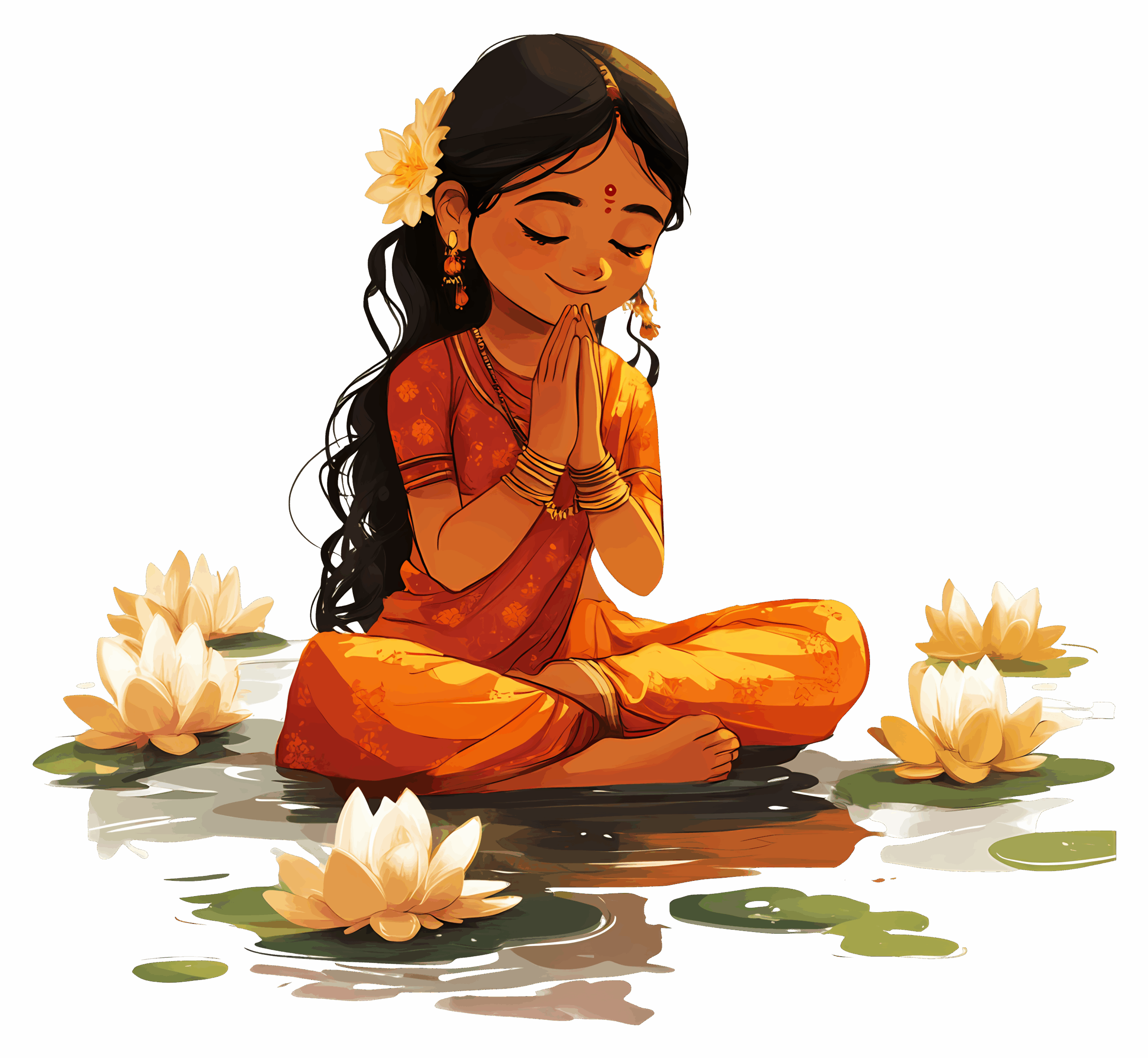
वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविद्य व्रत, पूजा, सन्तानोत्पत्ति, ब्रह्मयज्ञादि महायज्ञोंसे तथा ज्योतिष्टोमादि यज्ञोंसे ब्रह्माभिव्यञ्जक शरीरकी अर्थात् देहेन्द्रियप्राणान्तः करणरूप जीवनकी प्राप्ति होती है। —
स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः।
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।।
(मनुस्मृति २. २८)
संस्काररूप आचारसे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, द्रव्य, देश और क्रियाकी शुद्धि होती है। —
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धेश्च मनसस्तथा।
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते।।
(शाण्डिल्यस्मृति १. ११)
ध्यान रहे; श्रीहरि त्रिगुणमयी मायाके द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, स्त्रुवादि करण, यागादि कर्म, मन्त्र, शाकल्यादि द्रव्य और फल – इन नौ रूपोंमें व्यक्त होकर निरूपित होते हैं। —
कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः।
द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवधोक्तोऽजया हरिः।।
(श्रीमद्भागवत १२. ११. ३१)
श्रौत – स्मार्तसम्मत संस्कारोंसे जीवनमें सत्त्वगुणका उत्कर्ष होता है। सत्त्वगुणका उत्कर्ष होनेपर देशकालादिकी शुद्धि होती है। इनकी शुद्धिसे मन सविशेष और निर्विशेष परमात्मामें समाहित होता है। परमात्मामें चित्तके समाहित होनेपर जीवको ब्रह्मात्मतत्त्वका एकत्वविज्ञान सुलभ होता है। ब्रह्मात्मतत्त्वके एकत्वविज्ञानसे अविद्यादि प्रतिबन्धोंका निरास और निरावरण आत्माका प्रकाश होता है।

त्रिगुण — सत्त्व, रजस् तथा तमस्
साङ्ख्य और साङ्ख्यगर्भित वेदान्तप्रस्थानके अनुसार सत्त्व, रजस् तथा तमस् – संज्ञक तीन गुण हैं। गुणानुरूप प्राणियोंकी गति, मति तथा स्थिति – शास्त्र, युक्ति तथा अनुभूतिसिद्ध है। विशुद्ध सत्त्वसे ध्यान, समाधि और अविप्लव विवेकख्याति तथा निर्वृतिरूपा मुक्ति सुलभ होती है। मलिन सत्त्वसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणापर्यन्त निवृत्तियोग सुलभ होता है। रजोगुणसे अर्थ और कामपर्यवसायी धर्मानुष्ठानोंमें प्रीति तथा प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। तमोगुणकी प्रगल्भतासे निद्रा, आलस्य, प्रमाद या हिंसादि क्रूर कर्मोंमें प्रीति तथा प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
आगम (शास्त्र), अन्न – जल, प्रजा (सङ्ग), देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार — ये दस गुणमें हेतु हैं।
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च।
ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः।।
(श्रीमद्भागवत ११. १३. ४)
जिनका चित्त असंस्कृत है, वे इस रहस्यको नहीं समझ पाते कि जीवकी संस्कृति अविद्या, काम और कर्म हेतु हैं। सम्यग्दर्शनसम्पन्न आत्मनिष्ठ ध्यानयोगी अविद्यामूलक कर्मबन्धसे विनिर्मुक्त होते हैं, न कि सम्यक् – दर्शनविहीन। —
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयामकृतात्मभिः।
ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः।।
(मनुस्मृति ६. ७३)
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते।
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते।।
(मनुस्मृति ६. ७४)

व्यासस्मृतिके अनुसार गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपनक्रिया या चूडाकरण, कर्णवेध, उपनयन (व्रतादेश), वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, विवाहाग्निपरिग्रहण तथा त्रेताग्निसङ्ग्रह – नामक प्रसिद्ध षोडशसंस्कार हैं। —
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।
नामक्रियानिष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया।।
(व्यासस्मृति १. १३)
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः।
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः।।
(व्यासस्मृति १. १४)
त्रेताग्निसङ्ग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः।
(व्यासस्मृति १. १५ (१/२))

संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः।
प्राज्ञस्यानन्तरा सिद्धिरिहलोके परत्र च।।
(महाभारत — शान्तिपर्व २३५. २४)
“जो वैदिक संस्कारसे विधिवत् सम्पन्न है, जो नियमपूर्वक रहकर मन तथा इन्द्रियोंपर नियन्त्रण कर चुका है, उस प्राज्ञको लोक और परलोकमें कहीं भी सिद्धि प्राप्त करते देर नहीं लगती।।”
सनातनधर्ममें आहारादिरूप कामकी सिद्धिके लिये अनिन्द्य कर्मरूप धर्मका सम्पादन विहित है। आहारादिमें प्रवृत्ति विषयोपभोगकी लम्पटताके लिये नहीं, अपितु प्राणरक्षार्थ विहित है। प्राणसंधारण भगवत्तत्त्वकी जिज्ञासाके लिये विहित है। तत्त्वजिज्ञासा तत्त्वबोध प्राप्त कर दुःखोंके आत्यन्तिक उच्छेदकी भावनासे विहित है। —
आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्।
तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते।।
(श्रीमद्भागवत ११. १८. ३४)
अत्राहारार्थं कर्मकुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राणसंधारणार्थम्।
प्राणाः संधार्यास्तत्त्वजिज्ञासनार्थ तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्।।
(योगवासिष्ठ– निर्वाणप्रकरण २१. १०)

मोक्ष — धर्मका वास्तवफल
सनातनधर्म के अनुसार धर्म का वास्तव फल मोक्ष है। धर्मानुष्ठानसे सुलभ अर्थके द्वारा धर्मानुष्ठान और तत्त्वचिन्तनके अनुरूप जीवनकी समुपलब्धि विहित है। अर्थका विनियोग विषयलम्पटताकी परिपुष्टिमें निषिद्ध है।
धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते।
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः।।
(श्रीमद्भागवत १. २. ९)
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता।
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः।।
(श्रीमद्भागवत १. २. १०)
अर्थ, धर्म, काम और मोक्षको वास्तव पुरुषार्थका रूप प्रदान करने के लिये चारोंके मलका शोधन आवश्यक है। फलेच्छा धर्मका मल है, सङ्ग्रह अर्थका मल है, आमोद और प्रमोद कामका मल है और द्वैताभिनिवेश मोक्षका मल है। —
अपध्यानमलो धर्मो मलोऽर्थस्य निगूहनम्।
सम्प्रमोदमलः कामो भूयः स्वगुणवर्जितः।।
(महाभारत — शान्तिपर्व १२३. १०)
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्
(श्रीमद्भागवत ११. २. ३७, ३८)
यद्यपि आत्मदेव अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही है; तथापि अनादि अविद्या, काम और कर्मके वशीभूत प्राणी आत्मस्वरूपमें अध्यस्त अनात्मप्रपञ्चरूप द्वैतमें सत्ता, चित्ता और प्रियताका आधान कर व्यवहार दशामें अहन्ता ममतारूप अभिनिवेशके कारण भयको प्राप्त होता है। यद्यपि मृत्युग्रस्त, जड, दुःखप्रद देहादि विषम और सदोष अनात्मवस्तुओंमें अहंता – ममताशून्य सुषुप्तिमें भी द्वैतबीज अज्ञान विद्यमान रहता है, परन्तु द्वैताभिनिवेशके अभावमें अन्यमें अन्यबुद्धिरूप अध्यासरहित द्वैत भयप्रद नहीं होता। यद्यपि व्यवहारदशामें ग्राह्य और उपेक्ष्य वस्तुएँ भी द्वैत हैं, परन्तु वे तत्काल भयप्रद सिद्ध नहीं होती; तथापि उनकी श्रमप्रदता, वियोगशीलता और उनसे उपरामताके कारण वे आत्मस्वरूपमें अध्यस्त अवश्य हैं; अत एव वरणीय नहीं हैं, भयप्रद अवश्य हैं।
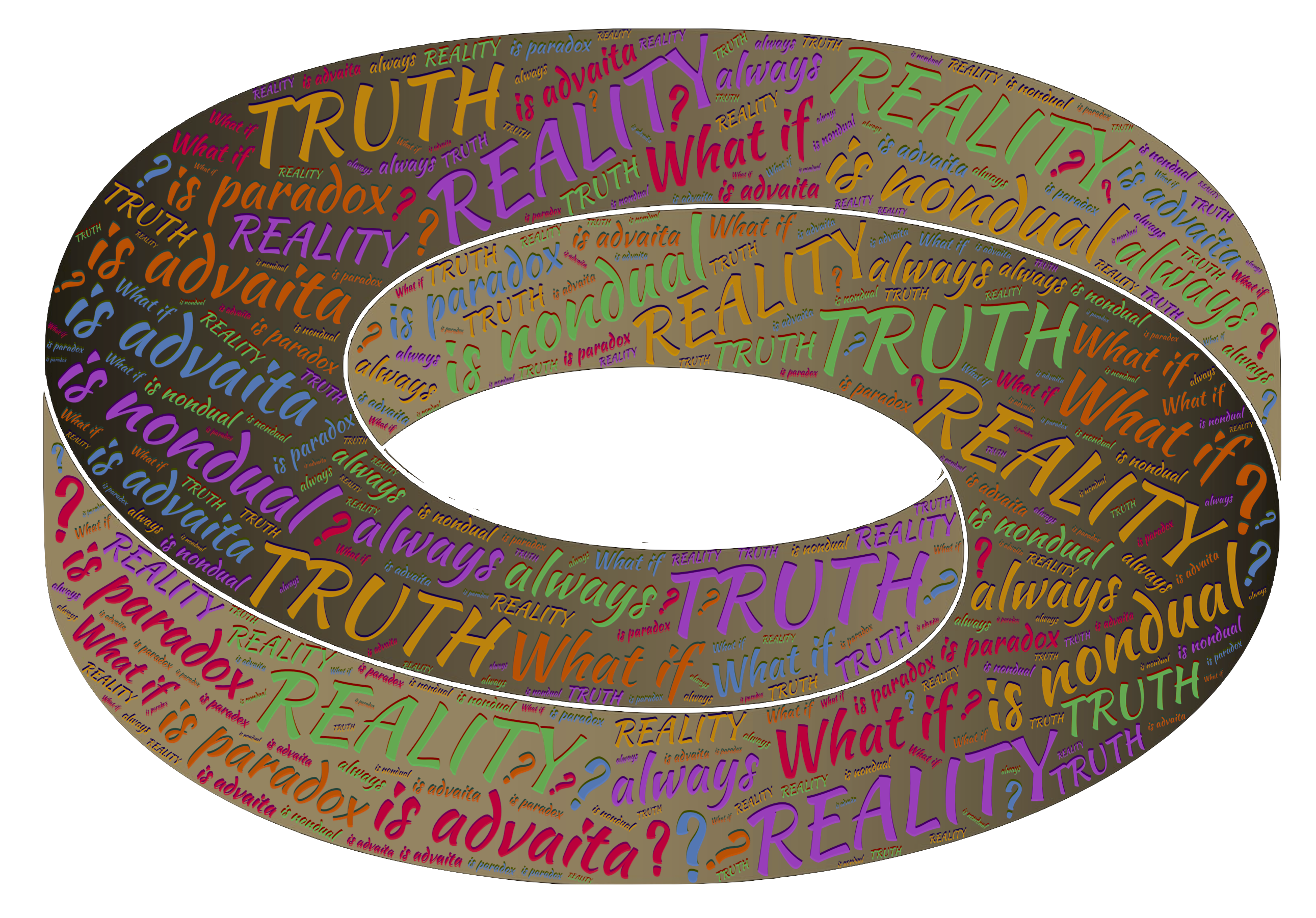
अभिप्राय यह है कि अनुकूल द्वैतकी भी स्थिर प्रेमास्पदता असिद्ध है, अतः भयप्रदता सिद्ध है। स्वप्न और मनोराज्यगत दृश्यप्रपञ्चके तुल्य ही बाह्यदृश्यका वास्तव अस्तित्व नहीं है। अतः द्वैत प्रपञ्चके अस्तित्वकी अभिमति (स्वीकृति) एवम् उसमें प्रीति और प्रवृत्ति तथा प्रतिकूलबुद्धिरूप अभिनिवेशसे मनको मुक्त कर सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मामें सन्निहित कर अभयप्रद मोक्षोपलब्धि ही जीवका चरम लक्ष्य और कर्त्तव्य है।
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या ५०९ – ५१८
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी
पुरुषार्थविहीनतासे रक्षा

(२) दूसरी विशेषता — प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणोंसे अनधिगत और अबाधित जगत् के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सच्चिदानन्द – स्वरूप सर्वेश्वरका नाम ब्रह्म है। उस सर्वेश्वरका उत्कर्ष दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर अनुपम है। अतः उसके भक्तोंका उत्कर्ष भी अद्भुत है। वह सर्वेश्वर सर्व, सर्वगत, सर्वान्तरात्मा, सर्वातीत तथा सगुण-निर्गुण-साकार-निराकार उभयरूप है। सनातन सर्वेश्वर वही है, जो सर्व जीवोंकी चाहका वास्तविक विषय सच्चिदानन्दस्वरूप है। वह आत्मीय ही नहीं; अपितु साक्षात् आत्मस्वरूप ही है। वह उसके अंश – सदृश सर्व जीवोंका आस्थास्पद और आकर्षणकेन्द्र अवश्य है। उसके वरणसे मृत्यु, अज्ञता, दुःखका आत्यन्तिक उच्छेद सुनिश्चित है। उसके साक्षात्कारकी भावनासे और विश्वको विप्लवपूर्ण विभीषिकाओंसे बचानेकी इच्छासे अर्थ और कामको पुरुषार्थविहीन होनेसे बचाना अत्यावश्यक है।

श्रीमद्भागवत ११. २३. १८, १९ के अनुसार चोरी, हिंसा, अनृत (झूठ), दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद (फूट), वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, लम्पटता, द्यूत (जूआ) और मद्य (मदिरा) रूप पन्द्रह अनर्थोंके चपेटसे अर्थको विमुक्त रखना परमावश्यक है। तद्वत् कामको देशातिक्रम (उचित देशका अविचार), कालातिक्रम (उचित कालका अविचार), पात्रातिक्रम (गम्य, अगम्यरूप पात्रताका अविचार), अशुचि, क्रोध, असंयम, निन्दा, वाचालता, अश्लीलता, मदविह्वलता, अभक्ष्यभक्षण, अतिसामीप्य, अतिदूरता, अस्निग्धता और अनुदारतारूप पन्द्रह दोषोंसे विमुक्त रखना परमावश्यक है।

तद्वत् धर्मको पुरुषार्थ-विहीनतासे बचानेके लिये अनधिकार चेष्टा, कालातिक्रम, देशातिक्रम, पात्रातिक्रम, दम्भ, द्रोह, अभिमान, ख्याति, असंयम, मिथ्या आहार-विहार, देवता-पितर-परलोक-परमेश्वर-परोपकार-पूर्वजन्म-पुनर्जन्ममें अनास्था, परोत्कर्षकी असहिष्णुता, आलस्य, असत्य और अधैर्यरूप पन्द्रह दोषोंसे विमुक्त रखना आवश्यक है। तद्वत् मोक्षको पुरुषार्थविहीनतासे बचानेके लिये पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, मलसहिष्णुता, विक्षेपसहिष्णुता, आवरणसहिष्णुता, प्रमाद, अहङ्कार, हरि-गुरुविमुखता, द्वैतसहिष्णुता, श्रवण मनन निदिध्यासनसे परामुखता, निर्गुण-निर्विशेषके अस्तित्वमें अनास्था, परमेश्वरकी परोक्षता, आत्माकी परिच्छिन्नता तथा असच्चिदानन्दरूपताकी मान्यतारूप पन्द्रह दोषोंका परित्याग परमावश्यक है।
— श्रीगोवर्द्धनमठ-पुरीपीठाधीश्वर-श्रीमज्जगद्गुरु-शंकराचार्य स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वती
द्वारा लिखित पुस्तक “नीतिनिधि” पृष्ठ संख्या ५१८ – ५१९
* साभार: श्री सुमित शर्मा जी (पिलानी) — इस लेख में मूलपाठ के योगदान के लिए